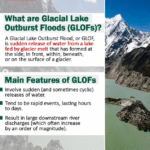चर्चा में क्यों?
हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर निर्देश जारी किए हैं, जिनमें राजनीतिक निष्पक्षता और सूचना गोपनीयता को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इसी संदर्भ में LBSNAA (लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी) ने भी अप्रैल 2025 में नवचयनित सिविल सेवकों को सलाह दी है कि वे डिजिटल माध्यमों पर सोच-समझकर व्यवहार करें और किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचें।
यह निर्देश और सलाह इस ओर इशारा करते हैं कि डिजिटल युग में लोक सेवकों के लिए नैतिक डिजिटल आचरण की भूमिका अब पहले से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है।
लोक सेवा में नैतिक डिजिटल आचरण के प्रमुख स्तंभ
-
पारदर्शिता: डिजिटल संचार को स्पष्ट, सुलभ और जनसाधारण के लिए समझने योग्य होना चाहिए। पारदर्शिता से नागरिकों का सरकार पर विश्वास बढ़ता है।
-
उत्तरदायित्व: सिविल सेवकों को अपने डिजिटल कार्यों के लिए व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से जवाबदेह होना चाहिए। किसी भी डिजिटल गलती की ज़िम्मेदारी लेना नैतिकता का आधार है।
-
निष्पक्षता: किसी भी राजनीतिक विचार, मत या प्रचार से बचते हुए, ऑनलाइन मंचों पर निष्पक्ष छवि बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।
-
सत्यनिष्ठा: ईमानदारी, स्पष्टता और संयम डिजिटल नैतिकता की रीढ़ हैं। भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट सार्वजनिक विश्वास को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग की चुनौती
आज अधिकतर सिविल सेवक सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। यह एक ओर उन्हें आम जनता से जुड़ने और नीतियों की जानकारी साझा करने का माध्यम देता है, वहीं दूसरी ओर इससे जुड़ी चुनौतियाँ भी हैं — जैसे:
-
व्यक्तिगत विचारों के कारण सेवा की निष्पक्षता पर सवाल।
-
संवेदनशील जानकारी के अनजाने में लीक होने का खतरा।
-
संस्थागत छवि को क्षति पहुँचने का जोखिम।
विनियमन के पक्ष में तर्क
-
राजनीतिक तटस्थता बनाए रखना
सिविल सेवकों को संविधान के अनुरूप गैर-राजनीतिक रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर राजनीतिक विचार व्यक्त करने से उनकी निष्पक्षता पर प्रश्न उठ सकता है। -
सूचना गोपनीयता की रक्षा
सोशल मीडिया के माध्यम से संवेदनशील सूचनाओं के लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। -
संस्थानिक गरिमा बनाए रखना
लोक सेवक सरकार का चेहरा होते हैं। उनकी ऑनलाइन गतिविधियाँ यदि गैर-पेशेवर हों, तो इससे संस्था की छवि प्रभावित होती है। -
जनहित प्रथम
गांधीवादी और उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुसार, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से ऊपर जनकल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
अति-विनियमन के विरोध में तर्क
-
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव
अत्यधिक नियंत्रण अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्राप्त अधिकार का हनन हो सकता है। जब तक कोई वास्तविक हानि न हो, स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए। -
पारदर्शिता में बाधा
सोशल मीडिया पर सिविल सेवकों की सक्रियता से जनता को सरकारी निर्णयों और कार्यप्रणाली की जानकारी मिलती है। अत्यधिक नियंत्रण से यह प्रक्रिया बाधित हो सकती है। -
नवाचार और जवाबदेही में कमी
जैसे केरल बाढ़ के समय IAS अधिकारी प्रशांत नायर ने सोशल मीडिया के माध्यम से राहत कार्यों का समन्वय किया — ऐसे नवाचार को नियंत्रित करने से प्रशासनिक कुशलता प्रभावित हो सकती है। -
पीढ़ीगत असंतुलन
युवा सेवक तकनीक में दक्ष हैं। यदि सोशल मीडिया पर अत्यधिक प्रतिबंध लगाए जाएँ, तो यह पीढ़ीगत दूरी और असंतोष को जन्म दे सकता है।
नैतिक डिजिटल आचरण के लिए सुधारात्मक उपाय
-
स्पष्ट दिशा-निर्देशों का निर्माण
यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ऑनलाइन आचरण में क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। इससे भ्रम और विवाद की स्थिति से बचा जा सकता है। -
रचनात्मक उपयोग को बढ़ावा
सोशल मीडिया का उपयोग जनजागरूकता, नीति प्रचार और जनता से संवाद के लिए किया जा सकता है। नैतिक उपयोग को प्रोत्साहन देना ज़रूरी है। -
डिजिटल नैतिकता का प्रशिक्षण
सभी स्तरों के सरकारी कर्मचारियों को डिजिटल आचरण, डेटा सुरक्षा और नैतिक संवाद पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। -
विभाग-विशिष्ट नीति
प्रत्येक मंत्रालय अपनी ज़रूरतों के अनुसार सोशल मीडिया नीति बना सकता है, जिससे कार्य-संवेदनशीलता बनी रहे। -
स्तरीकृत उत्तरदायित्व प्रणाली
सभी उल्लंघनों पर एक जैसा दंड न हो। चेतावनी से लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई तक अनुपातिक प्रतिक्रिया प्रणाली अपनाई जाए। -
आत्म-नियमन को बढ़ावा
संयम, शालीनता और सत्यनिष्ठा जैसे सद्गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। आत्म-अनुशासन ही दीर्घकालिक समाधान है।
निष्कर्ष
डिजिटल युग में सिविल सेवकों के लिए नैतिक डिजिटल आचरण एक नई आवश्यकता बन चुका है। उन्हें अभिव्यक्ति और उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और संयम के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। कोई भी विनियमन ऐसा न हो कि वह नवाचार, पारदर्शिता या सार्वजनिक संवाद को बाधित करे।